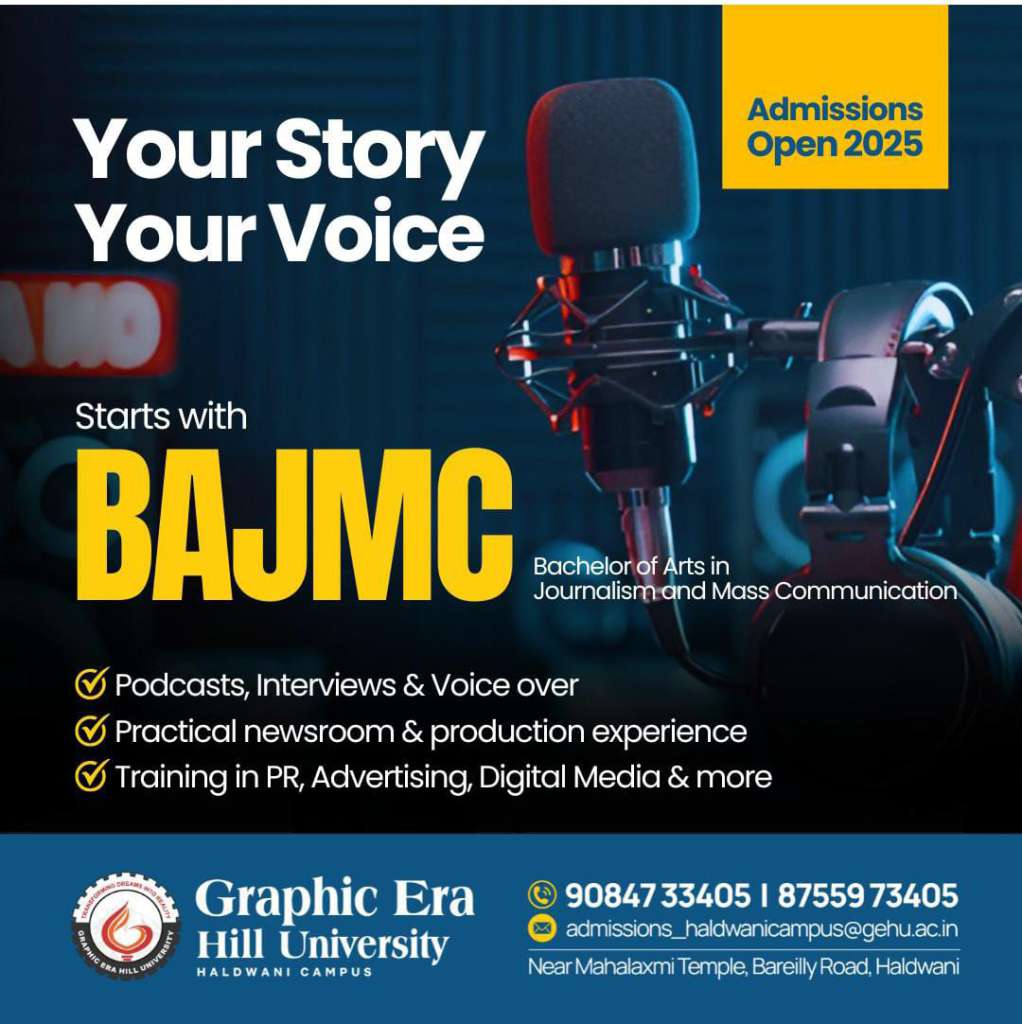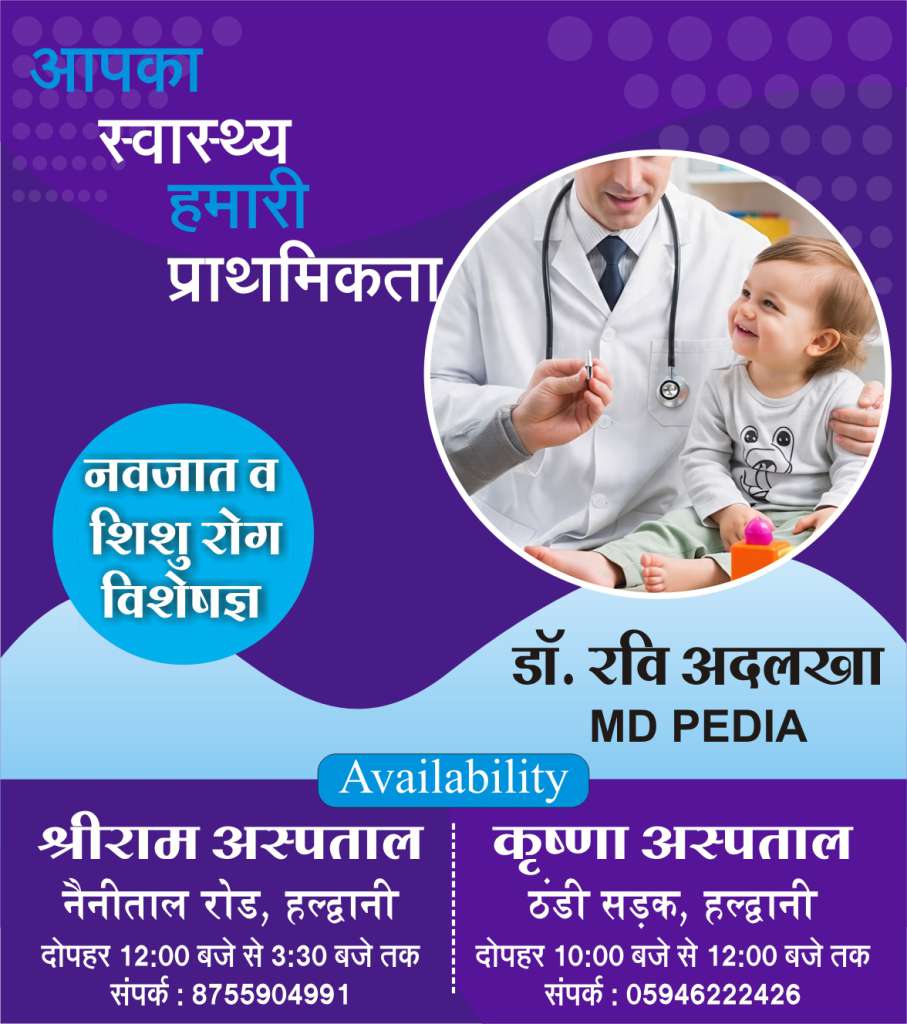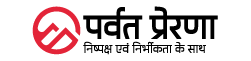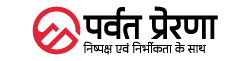उत्तराखण्ड
पहाड़ों से पलायन के कारण गैरसैंण से छीन गया राजधानी बनने का सपना
देहरादून। राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों आंदोलनकारियों ने जनपक्षीय और संतुलित विकास के सपने देखे परन्तु 22 सालों में यहां के राजनेताओं और नौकरशाहों की ठाठबाट की जीवन शैली ने स्वप्नों को धूमिल कर दिया है।
चुनावों में नेतागणों ने उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश, पर्यटन प्रदेश, एशिया का स्विटजरलैंड, शिक्षा का हब, देश की सांस्कृतिक राजधानी, और भी न जाने क्या-क्या बनाने के वादे कर दिए और अब उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार कहती है कि 2020 का दशक उत्तराखंड का दशक है, यही नहीं 2030 और 2040 की बात भी होने लगी है। गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने के आंदोलनकारियों के संकल्प को कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकी है।
आज से 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल से पहली बार राजधानी के बाबत गैरसैंण की ओर राज्य की सरकारों का रुख थोड़ा सकारात्मक हुआ, हालांकि ये कभी भी साफ नहीं हो पाया कि गैरसैंण(भराड़ीसैंण)में स्थाई राजधानी का निर्णय कब लिया जाएगा, पर जहां तक भाजपा सरकार का रुख है, वह गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्म कालीन राजधानी के तौर पर मान्यता देने का है, इसकी परिणति देहरादून को स्थाई राजधानी के रूप में ही हो सकती है।
22 साल के बाद गैरसैंण में उत्तराखंड की एकमात्र राजधानी बनाने का स्वप्न लगभग ध्वस्त कर दिया गया है। प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र के गांवों से 1990, 2000 और 2010 के दशकों के बाद 2020 के दशक में भी असामान्य गति से पलायन होना दून से दिल्ली तक के सत्ताधीशों की चिंता का विषय है। गांवों के निर्जन होने की तस्वीर वाकई डरावनी है।
2011 की जनगणना में उत्तराखंड में 1053 गांवों को निर्जन गांवों के तौर पर दर्ज किया गया और जनवरी 2018 में उत्तराखंड पलायन आयोग ने भुतवा हो चुके गांवों की संख्या 1064 बताई, इसके साथ की 650 गांवों की जनसंख्या में 50 प्रतिशत से भी अधिक की गिरावट पर सरकार को चेताया।
तेज गति से पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार के साधनों का अभाव, उसके बाद शिक्षा और फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी बताए गए हैं। कुछ गांव प्राकृतिक आपदा के कारण खाली हो चुके हैं। ये ऐसे कारण हैं जिनको दूर करने के लिए सरकार के प्रयास काफी निर्णायक हो सकते हैं, परन्तु सिवाय जुबानी खर्च के असामान्य गति के पलायन पर नियंत्रण के लिए कारगर नीतियों का निर्माण करने में सरकारें अब तक विफल हैं।
प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी भागों में अनियोजित विकास और हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल मात्र चार जिलों में ही रोजगार और सुविधाओं के अवसरों के सिमट जाने से इन्हीं चार जिलों में राज्य की आबादी का बड़ा भाग सिमट चुका है।
गौर करने वाली बात है कि पर्वतीय क्षेत्र से बहते प्रचुर पानी के उपयोग की हालत में भी बीते 22 सालों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सका है। जो कुछ सफलता बांधों के जरिए जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के क्षेत्र में मिली है वे लगभग सभी परियोजनाएं राज्य निर्माण से पहले शुरू हो चुकी थीं या उनके शुरुआत के लिए प्रक्रिया गतिमान थी। राज्य की सरकारें तो वक्त पर कई प्रस्तावित परियोजनाओं की डीपीआर तक तैयार नहीं करवा पाई। इसके साथ ही परियोजना प्रभावित स्थानीय लोगों को उनके जल, जंगल, जमीन के सवालों को हाशिए पर डाल, पर्यावरण प्रभाव पर अंधेरे में रखने की निजी विकासकर्ताओं की कार्यशैलियों ने उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर विरोध को बढाया है। इसकी वजह से कई छोटी-छोटी विवाद रहित परियोजनाएं भी प्रभावित हुईं फलस्वरूप आज भी उत्तराखंड का ऊर्जा में सरप्लस राज्य का स्वप्न अधूरा है। यही नहीं सभी घरों की शुद्ध पेयजल जैसी प्राथमिक जरूरत को भी सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है।
भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2004-05 में उत्तराखंड में 767 हजार हेक्टेयर था जो घटकर 2018-19 में 648 हजार हेक्टेयर हो गया। 14 साल में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में यह 119 हजार हेक्टेयर की कमी है, यानी हर साल औसतन साढे आठ हजार हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र कम होता गया। शुद्ध बोए गए रकबे में लगातार आई इस कमी का अर्थ है कि लोग लगातार खेती छोड़ रहे हैं, बंजर जमीन बढ रही है और इसके साथ ही खेती की जमीन विकास की भेंट चढ रही है। प्रदेश में कृषि योग्य जमीन कम होने से उसके उपयोग के लिए फूंक-फूंक कर कदम रखना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए केन्द्रीकृत तौर पर आगे आने वाले तीन-चार दशकों को ध्यान में रखकर योजना बनाने की जरूरत है, पर इस दिशा में राज्य सरकार कतई सक्रिय दिखाई नहीं देती।