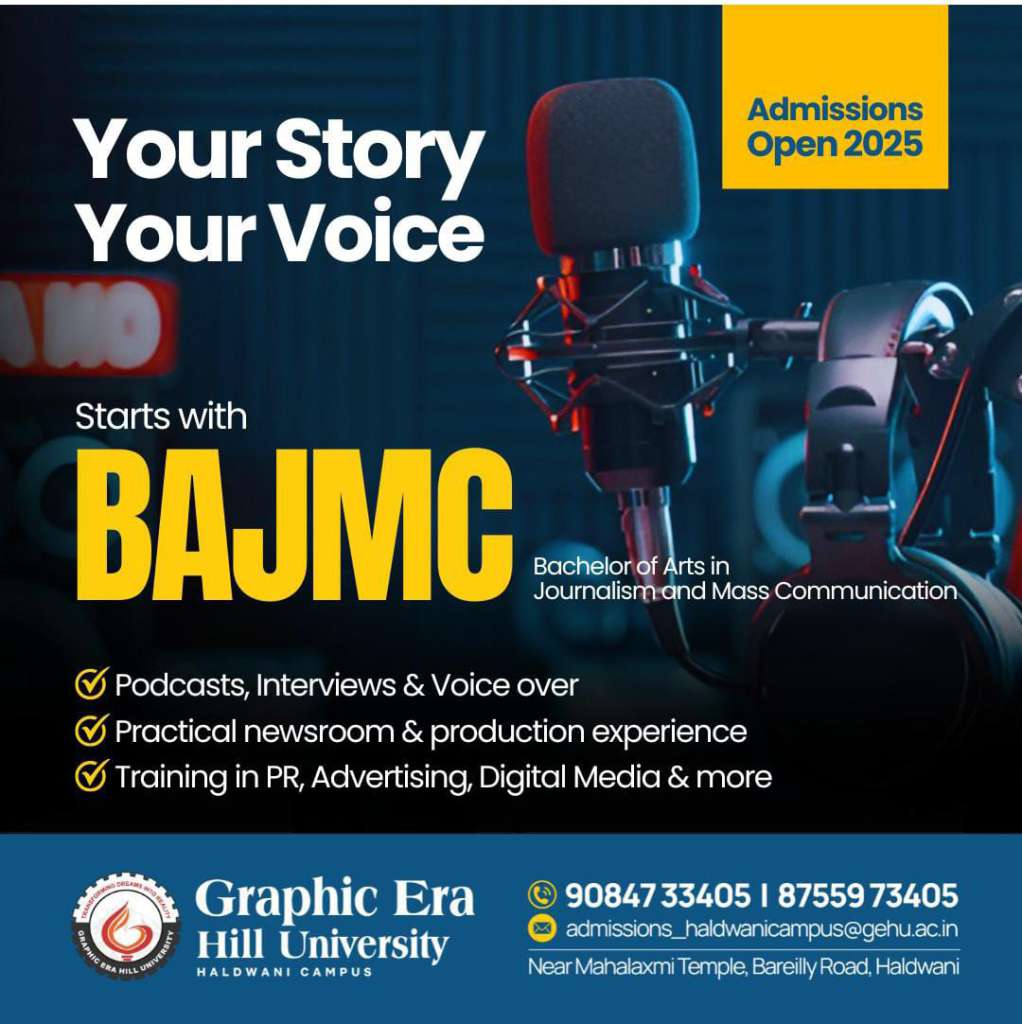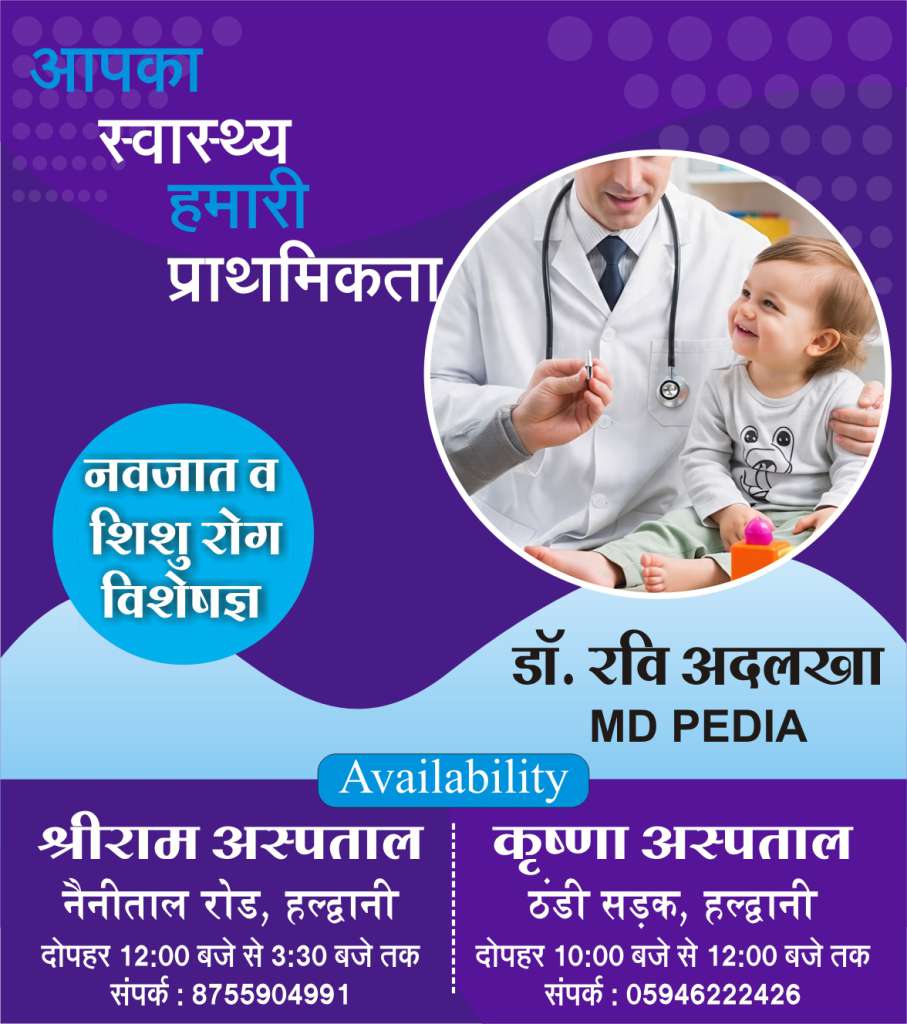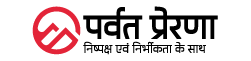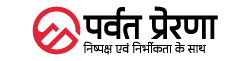कुमाऊँ
रामलीला मंचन की कल से अधिक आज जरूरत
प्राचीनकाल से ही उत्तराराखण्ड का सम्बन्ध रामभक्ति परम्परा से रहा है।पौराणिक श्रीराम कथा के आदि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में, इस प्रदेश को लक्ष्मण के पुत्रों को राज्य के रूप में प्रदान करने का उल्लेख है “जो रमणीय और निरायमय है. तब से, अर्थात् आज से दो हजार वर्ष पहले से ही बहुत पूर्वकाल से श्रीराम-लक्ष्मण, सीता, हनुमान आदि की पूजा का यहां प्रचार होना माना जाता हैं। सबसे पहले बरेली और मुरादाबाद में कुमाऊंनी तर्ज पर 1830 में रामलीला आयोजित हुईं और फिर सन् 1860 में अल्मोड़ा में रामलीला का मंचन किया गया था।
जनश्रुति है कि दुर्गा साह जी के प्रयत्नों से सन् 1897 में रामलीला का प्रथम मंचन नैनीताल में हुआ.इसी तरह सन् 1930 में शिव लाल शाह द्वारा रामलीला का मंचन बागेश्वर में प्रारम्भ किया. ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जानकीनाथ जोशी के प्रयत्नों से 1931 में शिमला में कुमाऊंनी रामलीला का प्रदर्शन किया गया।
कुमाऊं की रामलीला को अधिक समृद्ध और उत्कृष्ट बनाने में नृत्य सम्राट उदयशंकर के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है. उनके संगीतज्ञ के अनुभव ने रामलीला में नृत्य की मुद्राओं, पैरों के संचालन, लय-ताल तथा स्वर-संगीत का जो प्रयोग किया गया वो दर्शकों को बांधने में सफल रहे.
यह रामलीला गीत-नाट्य शैली में होने के कारण अन्य रामलीलाओं से अलग थी। वास्तव में इस रामलीला का सबसे महत्तवपूर्ण पक्ष इसका संगीत है. यहां की रामलीला पर शास्त्रीय संगीत का प्रबल प्रभाव है.रामलीलाओ में पहले कई शास्त्रीय शैली का प्रयोग किया जाता था। समय के साथ -साथ वाद्य यंत्रों में अब सिर्फ बांसुरी, हारमोनियम, तबला और वायलिन प्रयोग में लाए जाते हैं. गीतों के अतिरिक्त दोहों और चौपाइयों की एक विशेष संगीतात्मक शैली होती है।दोहे, चौपाइयां, गज़ल, गीत, सोरठा, शेर आदि शैलियां संगीत में प्रयोग की जाती हैं. ये सभी शैलियां अभिनेताओं (पात्रों) के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं।नाटक के सम्वादों का सबसे अधिक प्रयोग चौपाई शैली में होता है. परशुराम लक्ष्मण से संवाद (कुमाऊंनी) कहते हैं।
अब त्यरो मरण आइ गोछ रे छ्वारा, तसी जिबडी काटी यूंलो गंवारा.
तू क्या जाणं छै करतब म्यारा, धरती माजा मैंले छेतरीनी ध्यार .(यह हिंदी भाषा के रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार….)का कुमाऊनी भावार्थ है। इसी प्रकार अतीत में इसके संवर्धन के लिए प्रयोग होते गए।
गढ़वाल में मुख्यतः टिहरी, देवप्रयाग, पौड़ी, सुमाड़ी, देहरादून, और श्रीनगर की रामलीलाएं समृद्ध और प्राचीन मानी जाती हैं. टिहरी की रामलीला के सम्बन्ध मे विद्यासागर नौटियाल कहते हैं कि, “सन् 1933 में राजा नरेन्द्रशाह की रानी इंदुमति शाह दिल्ली से नरेन्द्र नगर अपनी कार मे लौट रही थी कि अचानक मुजफ्फनगर के पास कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई. कार वो स्वयं चला रही थीं. उन दिनों टिहरी में हर साल की तरह रामलीला की तैयारियां चल रही थी. खबर के टिहरी में पहुंचते ही शोक का वातावरण छा गया. उस मौत के कारण हमेशा के लिए हाड़ पड़ गया था. रियासत के अंदर रामलीला खेले जाने पर हमेशा के लिए पाबंदी लग गई.” इस तरह राजशाही सामंत ने अपने स्वार्थों के चलते रामलीला को निगल लिया. इससे पूर्व रियासत के अन्दर रामलीला के राज्यभिषेक दृश्य पर भी पाबन्दी लगाई गई थीं जिसके कारण कई रामलीलाएं का मंचन हमेशा के लिए बन्द हो गया था. तदनंतर टिहरी में वर्ष 1951 में “नवयुवक अभिनय समिति” की स्थापना की गई और पुनः रामलीला शुरू हो गई।
गढ़वाल में रामलीलाओं के इतिहास में पौड़ी की रामलीला प्रचीनतम रामलीलाओं में से एक है. सर्वप्रथम यहां सन् 1897 में रामलीला की शुरूवात की गई ।इस रामलीला की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता यह है कि सन् 2002 में पहली बार बालिकों को स्त्री पात्रों की भूमिका के लिए मंच पर उतारने का प्रयोग किया गया जिसकी परिपाटी आज तक भी बिना किसी गतिरोध के कायम है. यह लीला गैय शैली और शास्त्रीय संगीत पर आधारित है. रामलीला में आधुनिक तकनिकों का प्रयोग खुलकर होता है.
गढ़वाल में श्रीनगर की रामलीला का धार्मिक अनुष्ठान की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है. यह रामलीला सदियों से दशहरे में ही होती आई है. देवप्रयाग की रामलीला के संबंध में जय प्रकाश पंडित कहते है, देवप्रयाग के अधिकांश पंडित व्यवसाय के लिए बद्रीनाथ जाते है और मंदिर के कपाट बन्द होने के पश्चात ही वापस लौटते हैं इसलिए यहां रामलीला अक्टूबर में होती आई है. पहले रामलीला का आयोजन दस दिन का होता था अब पन्द्रह दिन का मंचन होता है. रामलीला आरंभ होने से पूर्व मुख्य पात्रों को वरणी दी जाती है ताकि वो कुछ खास बन्धनों में रहकर रामलीला करने के लिए प्रतिबद्ध रहें. इस रामलीला से एक मान्यता यह जुड़ी हुई है कि जिसके बच्चे नहीं होते है वे राजा दशरथ की भूमिका करते है और उन्हें पुत्र प्राप्त होती है.देहरादून कई रामलीला समितियों के उदय का केन्द्र रहा है परन्तु वर्तमान में दो-तीन समितियां ही कार्यरत हैं. देहरादून की सबसे प्राचीनतम संस्था “श्रीरामलीला कला समिति” लगभग 140 वर्षों से रामलीला का सफल मंचन करती आ रही है. रामायण का संक्षिप्त रूप है रामलीला जिसमें कुछ मुख्य घटनाओं को ही मंचित किया जाता है राम, लक्ष्मण आगमन, वनवास, मृग वध, सीता हरण, लंका दहन और महाभारत, नरसिंह, भक्त प्रहलाद, मोर, नंद, आदि। पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल किया जाता है. रामायण की यह दुर्लभ विधा विश्व में कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती है।
हां ये जरूर है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार लीला के मंचन में बदलाव अवश्य आ रहे हैं. कई रामलीलाओं के मंचन को सौ वर्ष से अधिक समय हो गया है पर संरक्षण के नाम पर आश्वसन के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता है. क्यों नहीं इन लीलाओं का मेले-त्योहारों के रूप आयोजन होता है ? क्यों नहीं इन रामलीलाओं को स्कूली पाठ्य पुस्तकों शामिल किया जाता है? क्या यह जरूरी कि जब तक कोई नाट्य विधा अपने मरने के कगार पर न पहुंचे तब तक उसके बारे सोचा न जाए?रामलीला हमारी संस्कृति का एक अंग हैं। हमारी परवरिश में जिन आदर्शों, मुल्यों व चरित्रों का योगदान रहा हैं रामलीला उनमें प्रमुख है। रामलीला आज भी नही बदली है, बदली हैं तो उसको देखने का दृष्टिकोण। इंटरनेट व तकनीकी के बढते प्रचार, प्रसार व उपयोग ने हमें कसकर पकड़ रखा हैं। हम बिना अपराध किये सजाएं-ए- कैद हो गए हैं। और भरी महफ़िल में भी तन्हा-तन्हा से लगते है। आज स्थिति ये हो गयी हैं कि हम घर में तो है लेकिन घर में नही हैं। हमारा घर पर होना ना होना बराबर हैं। कोई एक कोना पकड़े बैठें हैं और सोशल मीडिया के जाल में फँसते जाते है। हमें लगता हैं हम आनंद उठा रहे है जबकि होता ये है कि हम गवां रहे होते है। तकनीकी व प्रौद्योगिकी की अधिकता ने हमें शारारिक सक्रियता से अलग-थलग, पृथक कर दिया है। हम काल्पनिक रूप से जी रहे होते है। हकीकत से रूबरू नही हो पाते। रामलीलाओं की खूबसूरती इनमें देखी तो जा सकती हैं, महसूस नही की जा सकती। उसके लिए रामलीलाओं के मंचन तक चलना होगा, जाना होगा। रामलीला जहाँ हमें स्वस्थ्य मनोरंजन देती है वही गुज़रे कल की यादों की डोर से बाँधे भी रखता हैं।
हम एक साथ भूत व वर्तमान में हो रहे होते है। ये इसी का प्रभाव हैं कि हम अगली पीढ़ी को भी इससे परिचित कराना चाहते हैं। यानि हम इसे भविष्य में भी देखना चाहते हैं। रामलीला में हम दिलखोलकर, लोट-पोट कर हँसते है, हँसाते है। बदलते वक़्त में अगर किसी कार्यक्रम , आयोजन से हम ख़ुश रह सकते है, उसकी बातें कर सकतें है, उसको सांझा कर सकते है और समेटकर रख सकते है तो वह रामलीला ही है। अगर रामलीलाओं का मंचन खूबसूरती के साथ किया जाय तो आज भी यह लोगों को आकर्षण करने की क्षमता रखती है। स्थानीय व घरेलू यहां तक की ग्राउंड जीरो लेवल पर कलाकारों, गायकों, वाद्य यंत्र बजाने वालों, हँसाने वालों, स्वांग रचने वालों, चित्रकारों,साज-सज्जा करने वालों इत्यादि फ़नकारों को अपने कौशल, प्रतिभा,शऊर दिखाने का सबसे बढ़िया, नज़दीक व मज़बूत मंच रामलीला प्रदान करता है। कई कलाकारों ने रामलीलाओं के मंचन से राष्ट्रीय फलक तक में अपनी पहचान बनाई है। इसीलिए रामलीलाओं का मंचन जरूर किया जाना चाहिए और खूबसूरती के साथ किया जाना चाहिए।
सरकार व औद्योगिक घराने को भी इस दिशा में आगे आकर रामलीला पर प्रायजको, आयोजनकर्ताओं, प्रबंधको, कलाकारों के साथ समन्यव बनाये रखें तो कोई बात नही रामलीला आज भी अर्थ देते नजर आयेगी।
प्रेम प्रकाश उपाध्याय ‘नेचुरल’
पिथौरागढ़, उत्तराखंड
(लेखक सांस्कृतिक, सामाजिक व शैक्षणिक सरोकारों से जुड़े हैं)